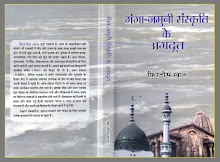फ़िरदौस ख़ान
दुनिया की क़रीब आधी आबादी महिलाओं की है. इस लिहाज़ से महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में बराबरी का हक़ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. कमोबेश दुनियाभर में महिलाओं को आज भी दोयम दर्जे पर रखा जाता है. अमूमन सभी समुदायों में महिलाओं को पुरुषों से कमतर मानने की प्रवृत्ति है. भारत में ख़ासकर मुस्लिम समाज में तो महिलाओं की हालत बेहद बदतर है. सच्चर समिति की रिपोर्ट के आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं कि अन्य समुदायों के मुक़ाबले मुस्लिम महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ख़ासी पिछड़ी हुई हैं, लेकिन काबिले-तारीफ़ बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद मुस्लिम महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित कर रही हैं.
सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक़ देशभर में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 53.7 फ़ीसदी है. इनमें से अधिकांश महिलाएं केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित हैं. सात से 16 आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली लडक़ियों की दर केवल 3.11 फ़ीसदी है. शहरी इलाकों में 4.3 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाकों में 2.26 फ़ीसदी लडक़ियां ही स्कूल जाती हैं. वर्ष 2001 में शहरी इलाकों में 70.9 फ़ीसदी लडक़ियां प्राथमिक स्तर की शिक्षा हासिल कर पाईं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह दर 47.8 फ़ीसदी है. वर्ष 1948 में यह दर क्रमश: 13.9 और 4.0 फ़ीसदी थी. वर्ष 2001 में आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाली शहरी इलाकों की लडक़ियों की दर 51.1 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाकों में 29.4 फ़ीसदी है. वर्ष 1948 में शहरी इलाकों में 5.2 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाकों में 0.9 फ़ीसदी लडक़ियां ही मिडल स्तर तक शिक्षा हासिल कर पाईं. वर्ष 2001 में मैट्रिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वाली लडक़ियों की दर शहरी इलाकों में 32.2 फ़ीसदी और ग्रामीण इलाकों में 11.2 फ़ीसदी है. वर्ष 1948 में यह दर क्रमश: 3.2 और 0.4 फ़ीसदी है.
शिक्षा की ही तरह आत्मनिर्भरता के मामले में भी मुस्लिम महिलाओं की हालत चिंताजनक है. सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक़ 15 से 64 साल तक की हिन्दू महिलाओं (46.1 फ़ीसदी) के मुकाबले केवल 25.2 फ़ीसदी मुस्लिम महिलाएं ही रोज़गार के क्षेत्र में हैं. अधिकांश मुस्लिम महिलाओं को पैसों के लिए अपने परिजनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके चलते वे अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर एक भी पैसा ख़र्च नहीं कर पातीं.
यह एक कड़वी सच्चाई है कि मुस्लिम महिलाओं की बदहाली के लिए 'धार्मिक कारण' काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं. इनमें बहुपत्नी विवाह और तलाक़ के मामले मुख्य रूप से शामिल हैं. इतना ही नहीं शरीयत की आड़ में उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है और जब भी कोई पीड़ित महिला अदालत के दरवाज़े पर दस्तक देती है तो उससे कठमुल्लाओं को तकलीफ़ होने लगती है. गौरतलब है कि पिछले साल 21 जनवरी को मुंबई की एक अदालत द्वारा तलाक़ के बारे में दिए गए फ़ैसले से भी कठमुल्लाओं की भवें तन गई थीं. उन्होंने अदालत के फ़ैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप क़रार देते हुए इसे मानने तक से इंकार कर दिया था.
पुरातनपंथी तुच्छ मानसिकता को त्याग कर मुंबई उच्च न्यायालय के फ़ैसले का खुले दिलो-दिमाग़ से स्वागत करना चाहिए था. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीएच मारलापाले ने दिलशाद बेगम द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया कि कोई भी व्यक्ति महज़ तीन बार तलाक़ कहकर अपनी पत्नी से संबंध नहीं तोड़ सकता है. दिलशाद बेगम को जून 1989 में उसके पति अहमद ख़ान पठान ने तीन बार तलाक़ कहकर घर से निकाल दिया था. इस मामले में पश्चिमी महाराष्ट्र के बारामती के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धाराओं के तहत हर्जाने के रूप में दिलशाद बेगम को चार सौ रुपये प्रति माह दिए जाने का आदेश दिया था. महज़ एक माह गुज़ारा भत्ता देने के बाद मई 1994 में दिलशाद के पति ने एक स्थानीय मस्जिद में जाकर उसे तलाक़ दे दिया था. साथ ही अहमद ख़ान पठान ने दिलशाद बेगम को दिया जाना वाला भत्ता भी बंद कर दिया और सेशन कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट के फ़ैसले को चुनौती भी दे डाली.
उसका तर्क था कि शरीयत (इस्लामी क़ानून) के मुताबिक़ तलाक़शुदा महिला को गुज़ारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है. इस पर सेशन कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को ख़ारिज कर दिया. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिलशाद बेगम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई, जहां उसे इंसाफ़ मिल गया. मगर यहां फिर कट्टरपंथियों ने उच्च न्यायालय के आदेश को मानने से इंकार करते जहां भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया वहीं, एक पीड़ित महिला के साथ भी ज़्यादती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सनद रहे 1981 में भी इसी तरह के एक मामले में न्यायमूर्ति मणिसेना और न्यायमूर्ति एसवी राम की खंडपीठ ने अनवरी बेगम को राहत देते हुए तलाक़ को अवैध क़रार दिया था. इस मामले में जियाउद्दीन ने एक बार तलाक़ कहकर ही अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था. अपना फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने शरीयत का हवाला भी दिया था.
गौर करने लायक़ बात यह भी है कि दिलशाद बेगम के मामले में अदालत की टिप्पणी शरीयत के मद्देनज़र भी जायज़ है. अदालत ने कहा है कि केवल तीन बार तलाक़ बोलकर ही कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक़ नहीं दे सकता. मौखिक या लिखित तलाक़ कहने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी समस्या के निपटारे के लिए तलाक़ कहने वाले व्यक्ति ने सुलह के प्रयास किए हैं. शरीयत के मुताबिक़ तलाक़ को एक बड़ा गुनाह माना गया है और इसे ख़ुदा की सबसे ज्यादा नापसंद चीज़ों में शामिल किया गया है. अगर हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि तलाक़ के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता तो इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं. इनके तहत पति और पत्नी के पक्ष का एक-एक व्यक्ति बातचीत के ज़रिये दोनों में सुलह कराने का प्रयास करेगा.अगर उन्हें इसमें कामयाबी न मिले तो वे क़ाज़ी के पास जाएंगे और क़ाज़ी उन्हें विचार-विमर्श के लिए तीन महीने का समय देगा. इस दौरान दोनों को एक ही घर में रहना होगा, ताकि समझौते की संभावना बनी रहे. अगर इस पर भी उनमें सुलह नहीं होती है तो क़ाज़ी उन्हें तलाक़ का हुकम देगा. क़ुरान शरीफ़ में कहीं भी एक साथ तीन बार तलाक़ कहने की बात नहीं कही गई है. मगर इसके बावजूद मुस्लिम समाज में पुरुष महिलाओं को तलाक़ देकर कभी भी घर से निकाल देते हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि मंजहब के ठेकेदार भी इसमें पुरुषों को भरपूर सहयोग देते हैं. हैरत की बात यह भी है कि क़ुरान को अल्लाह का आदेश बताने वाले कठमुल्ला महिलाओं पर अत्याचार के मामले में ईश्वरीय आदेश तक की अवहेलना करने से बाज़ नहीं आते. यह कहना ग़लत न होगा कि कठमुल्लाओं को न तो ईश्वर के आदेश की परवाह है और न ही भारतीय संविधान की, उन्हें तो महज़ अपनी 'दुकानदारी' चलानी है.
यह कोई पहला मामला नहीं है जब शरीयत के नाम पर किसी पीड़ित महिला पर ज़्यादती की गई हो. 1986 में शाहबानो ने अपने पति से गुज़ारा भत्ता पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था. याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया था उससे शाहबानो को तो कुछ राहत मिली थी, लेकिन यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे से बाहर चला गया था. दरअसल जिस धारा के तहत यह फ़ैसला सुनाया गया था, वह मुसलमानों पर (मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण) लागू ही नहीं होती थीं. नतीजतन, सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले पर काफ़ी हंगामा हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को लोकसभा में विधेयक लाकर इस फ़ैसले को आंशिक रूप से बदलना तक पड़ा था. इस विधेयक का मक़सद सिर्फ़ कठमुल्लाओं को ख़ुश रखना था.अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार चाहती तो सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले का सम्मान करते हुए इसे बरक़रार रख सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया.
गौरतलब है कि उड़ीसा के भद्रक की नजमा बीबी को उसके पति शेर मोहम्मद ने नशे की हालत में 15 जुलाई 2003 को तीन बार तलाक़ दे दिया था. इसी आधार पर कठमुल्लाओं ने उन्हें अलग रहने पर मजबूर कर दिया. इस पर दम्पति ने पारिवारिक अदालत की शरण ली और फ़ैसला उनके हक़ में रहा. इसके बाद भी कठमुल्लाओं के विरोध के चलते उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे ख़ारिज कर दिया गया. इस पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की. अदालत ने सुनवाई के बाद 21 अप्रैल 2006 को तलाक़ को अनुचित क़रार देते हुए उन्हें साथ रहने की अनुमति दी. साथ ही उडीसा सरकार को दम्पति को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया. मगर कठमुल्लाओं ने सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले को मानने तक से इंकार कर दिया. देवबंदी उलेमा ने तो यहां तक कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को इस्लामी शरीयत में दख़ल देने का कोई हक़ नहीं है.
इतना ही नहीं महिलाओं के ख़िलाफ़ फ़तवे जारी करना भी कठमुल्लाओं का एक शगल बन चुका है. 15 मार्च 2006 को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां ने जदीद की बरेली में हुई बैठक में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन का सिर क़लम करने वाले व्यक्ति को पांच लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. साथ ही उनके भारत में प्रवेश पर रोक लगाने और उनका वीज़ा समाप्त करने की मांग भी केंद्र सरकार से कर डाली. इस मौलाना ने पिछले साल अमेरिका के राष्ट्रपति डब्ल्यू जॉर्ज बुश का सिर कलम करने वाले व्यक्ति को 25 सौ करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. अदालती फैसलों पर टिप्पणी करते हुए तौक़ीर मियां ने यह भी चेतावनी दे डाली कि शरीयत (इस्लामी क़ानून) में किसी किस्म की भी दख़ल अंदाज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सहयोग देने पर मीडिया की सराहना करना तो दूर, बल्कि उन्होंने मीडिया पर ही कई आरोप जड़ डाले. इससे पहले कोलकाता के इमाम सैयद नुरूल रहमान बरकाती ने तस्लीमा नसरीन की मौत का फ़तवा जारी किया था.गत नौ अगस्त को हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (एमआईएम) के तीन विधायकों मौअज्ज़म ख़ान, मुक्तादा अफ़सर ख़ान और पाशा क़ादरी के नेतृत्व में भीड़ ने तसलीमा नसरीन पर हमला कर दिया और अगली बार हैदराबाद आने पर उनका सिर क़लम करने की घोषणा भी की.
बलात्कार के मामलों में भी पीड़ित महिलाओं पर अत्याचार करते हुए बलात्कारियों के पक्ष में फ़तवे जारी किए गए. जून 2005 में मुज़फ्फ़रपुर की इमराना को उसके ससुर अली मोहम्मद ने अपनी हवस का पक्ष में फ़तवा दिया था. फ़तवे कहा गया था कि वह अब अपने ससुर को पति मानेगी. इस रिश्ते से उसे अपने पति नूर इलाही को पुत्र मानना होगा. इमराना मामले में अदालत का फ़ैसला आने तक दो अन्य मुस्लिम महिलाओं ने इंसाफ़ के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटाया. मुज़फ़्फ़रनगर की ही 28 वर्षीय रानी के साथ भी उसके ससुर ने बलात्कार किया था. हरियाणा की भी एक महिला को उसके ससुर ने हवस का शिकार बनाया. इस हादसे के बाद पीड़ित महिला अपने मायके आ गई तो बलात्कारी ससुर उसके पति की हैसियत से उसे लेने तक पहुंच गया.
गौरतलब है कि शरीयत के मुताबिक़ किसी महिला का अपने पति के रक्त संबंधियों के साथ शारीरिक संबंध क़ायम हो जाने पर उसकी शादी की मान्यता ख़त्म हो जाती है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा संबंध बलात्कार नहीं होता.25 जुलाई 2006 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के गांव कंटाबागन की रेहाना के साथ वहीं के मंसूर मलिक ने बलात्कार किया. इस मामले में भी कठमुल्लाओं ने पीड़िता को प्रताड़ित करते हुए फ़ैसला सुनाया कि अब वह अपने पति की पत्नी नहीं रही और उसे बलात्कारी से निकाह करना होगा. शर्मनाक बात यह भी है कि रेहाना और उसके पति मुलुक शेख़ से कहा गया कि अगर वे 50 हजार रुपये मौलवी के पास जमा करा दें तो 'शरीयत' उन पर रहम करेगी, यानी सब खेल पैसों का है.
इसी तरह वर्ष 2006 में बिहार के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के गांव चांदवाडी में बलात्कार की शिकार एक गूंगी महिला को बच्चे को जन्म देने की वजह से नापाक क़रार दे दिया था. इतना ही नहीं कठमुल्लाओं ने दबाव बनाकर महिला को उसके पति के घर से निकलवा दिया. जब वह अपने पिता शमशेर अली के घर चली गई तो कठमुल्लाओं ने उसके पिता पर भी बेटी को घर से निकालने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, मगर जब वह नहीं माने तो कठमुल्लाओं ने उन्हें प्रताड़ित करते हुए गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उनका बहिष्कार करा दिया. हैरत की बात तो यह है कि बलात्कारी के ख़िलाफ़ कठमुल्लाओं ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुरुषों को सज़ा देने की बात पर कठमुल्ला शरीयत को भूल जाते हैं कि इस्लाम में बलात्कारी को सरेआम तब तक कोड़े मारने की बात कही गई है, जब तक की उसकी मौत नहीं हो जाती.
यह कहना क़तई ग़लत न होगा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को केवल भोग की वस्तु बनाकर रख दिया गया है. इसीलिए शरीयत का डंडा भी हमेशा महिलाओं के ख़िलाफ़ ही चलता है. फ़तवा चाहे तस्लीमा नसरीन के ख़िलाफ़ जारी हो या किसी अन्य पीड़ित महिला के ख़िलाफ़, सभी में अमानवीयता कूट-कूटकर भरी है. कठमुल्ला आए दिन फ़तवे जारी महिलाओं की ज़िन्दगी में ज़हर घोलते रहते हैं, लेकिन 14 करोड़ क़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में न तो किसी मुस्लिम संगठन ने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत की है और न ही छदम धार्मिक निरपेक्षता के चलते महिला आयोग या अन्य संगठन ने पीड़ित महिलाओं को सहारा दिया. कठमुल्लाओं का इतना खौफ़ है कि मार्च 2004 में मानवाधिकार आयोग ने भी नजमा बीबी के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था. मुसलमानों के मसीहा होने का दम भरने वाले और क़ौम की तरक्की के लिए सरकार से अनेक सुविधाओं की मांग करने वाले तथाकथित मुस्लिम नेता भी इस तरह के मामलों में दुबककर बैठ जाते हैं. जो नेता अपने क़ौम की महिलाओं पर अत्याचार होते देख ख़ामोश रहकर कठमुल्लाओं के हौसले बुलंद करते हैं, वे समुदाय का क्या भला करेंगे, यह वाक़ई समझ से परे है.
वर्ष 2006 में राजधानी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव व राज्यसभा सांसद महमूद मदनी ने मुस्लिम महिलाओं के ख़िलाफ़ जारी फ़तवों का समर्थन करते हुए कहा था कि मैं मुसलमान हूं और फ़तवों को मानने के लिए बाध्य हूं. यानी जो मुसलमान है, उसे फ़तवों को मानना ही पडेग़ा. अब जब क़ौम के रहनुमाओं की यह मानसिकता है तो अधिकांश अनपढ़ तबके से क्या उम्मीद की जा सकती है? हक़ीक़त यह भी है कि इसी तालिबानी मानसिकता ने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया.
हक़ीक़त यह है कि मज़हब के ठेकेदार 'शरीयत' की परिभाषा अपने स्वार्थ की पूर्ति के नजरिये से करते हैं. भारत में इस्लाम का जो रूप प्रचलित है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगम्बर हज़रत मुहम्मद उसे नापसंद करते थे. क़ुरान में महिलाओं को सम्मानजनक दर्जा दिया गया है. यहां तक कहा जाता है कि मां के क़दमों के नीचे जन्नत है. हज़रत मुहम्मद के वक़्त में भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए थे. वे मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढती थीं और पुरुषों की तरह ही घर से बाहर जाकर काम करती थीं. अनगिनत युध्दों में महिलाओं ने अपने युध्द कौशल का लोहा भी मनवाया. प्रसिध्द औहद की जंग में जब हज़रत मुहम्मद ज़ख्मी हो गए तो उनकी बेटी फ़ातिमा ने उनका इलाज किया.
उस दौर में भी रफायदा और मैमूना नाम की प्रसिध्द महिला चिकित्सक थीं. रफायदा का तो मैदान-ए-नबवी में अस्पताल भी था, जहां गंभीर मरीज़ों को दाख़िल किया जाता था. मुस्लिम महिलाएं शल्य चिकित्सा भी करती थीं. उम्मे ज़ियाद शाज़िया, बिन्ते माऊज़, मआज़त-उल-अपगारिया, अतिया असरिया और सलीम अंसारिया आदि उस ज़माने की प्रसिध्द शल्य चिकित्सक थीं. मैदान-ए-जंग में महिला चिकित्सक भी पुरुषों जैसी ही वर्दी पहनती थीं. हज़रत मुहम्मद की पत्नी ख़दीजा कपड़े क़ा कारोबार करती थीं. महिला संत राबिया की ख्याति दूर-दूर तक फैली थी. पुरुष संतों की तरह वे भी धार्मिक सभाओं में उपदेश देती थीं. सियासत में भी महिलाओं ने सराहनीय काम किए. रंजिया सुल्ताना हिन्दुस्तान की पहली महिला शासक बनीं. नूरजहां भी अपने वक्त क़ी ख्याति प्राप्त राजनीतिक रहीं, जो शासन का अधिकांश कामकाज देखती थीं.1857 की जंगे-आज़ादी में कानपुर की हरदिल अज़ीज़ नृत्यांगना अज़ीज़न बाई सारे ऐशो-आराम त्यागकर देश को गुलामी की ज़ंजीरों से छुड़ाने के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं. उन्होंने महिलाओं के समूह बनाए जो मर्दाना वेश में रहती थीं. वे सभी घोड़ों पर सवार होकर और हाथ में तलवार लेकर नौजवानों को जंगे-आंजादी में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थीं. अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हज़रत महल ने हिन्दू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए.
मौजूदा दौर में भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपनी योग्यता का परिचय दे रही हैं. तुर्की जैसे आधुनिक देश में ही नहीं, बल्कि कट्टरपंथी समझे जाने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश सरीखे देशों में भी महिलाओं को प्रधानमंत्री तक बनने का मौक़ा मिला है. वाक़ई यह एक ख़ुशनुमा अहसास है कि 'मज़हब के ठेकेदारों' की तमाम बंदिशों के बावजूद मुस्लिम महिलाएं आज राजनीति के साथ खेल, व्यापार, उद्योग, कला, साहित्य, रक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. जम्मू कश्मीर के कुलाली-हिलकाक इलाक़े की मुनिरा बेगम ने आतंकवादियों का मुंकाबला करने के लिए बंदूक़ उठा ली. उन्हीं के नक्शे-क़दम पर चलते हुए सूरनकोट के गांव की अन्य महिलाओं ने भी हथियार उठाकर आतंकवादियों से अपने परिजनों की रक्षा करने का संकल्प लिया. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की शबनम आरा ने तमाम अवरोधों को पार कर गांव के क़ाज़ी का पद संभाला.
इसमें दो राय नहीं कि आज मुसलमानों में ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो इस्लाम के उस वास्तविक रूप को सबके सामने रखना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद ही कुप्रथाओं के ख़ात्मे के लिए पड़ी थी. धर्म गुरुओं को भी चाहिए कि वे क़ौम को अज्ञानता और रूढ़ियों के अंधेरे से निकालने में महती भूमिका अदा करें. इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए आदर्श के रूप में पेश किया जाए, जिससे अन्य लडक़ियां भी प्रेरणा हासिल कर सकें.




















.jpg)